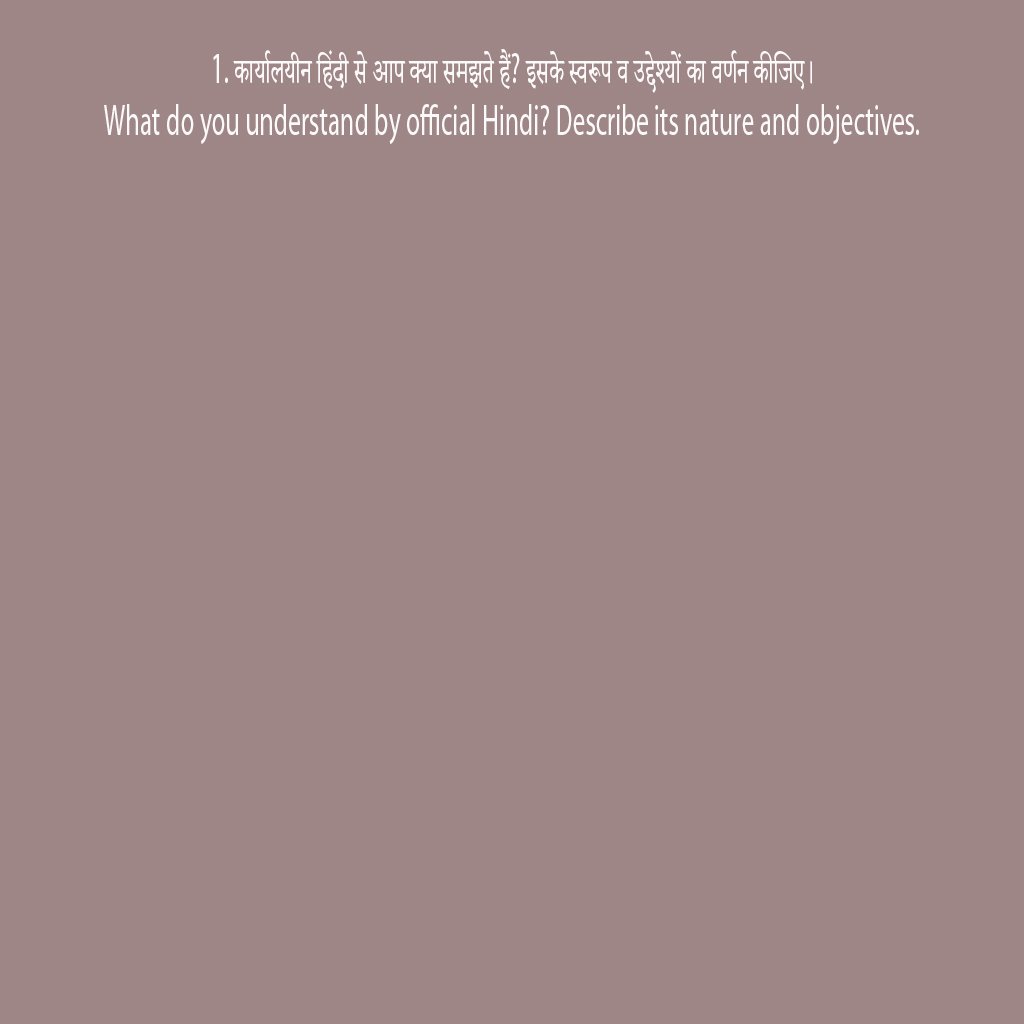कार्यालयीन हिंदी से आप क्या समझते हैं? इसके स्वरूप व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।What do you understand by official Hindi? Describe its nature and objectives.
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
भूमिका:
भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा का प्रयोग केवल संचार का माध्यम भर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, प्रशासनिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में एक समान, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग हो सके। कार्यालयीन हिंदी इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जो सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तरों में कार्य संपादन के लिए अपनाई गई है।
कार्यालयीन हिंदी की परिभाषा:
कार्यालयीन हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा अन्य संस्थानों के कार्यालयों में कार्य संचालन, प्रशासनिक कार्यों, पत्राचार, आदेश, अधिसूचना, प्रतिवेदन, स्मरणपत्र, प्रस्ताव, टिप्पणियों, फाइलों के नोट आदि के लिए किया जाता है।
यह एक ऐसी हिंदी है जो औपचारिक, स्पष्ट, संक्षिप्त तथा प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त हो। इसमें अनावश्यक अलंकार, कठिन शब्दों या साहित्यिक शैली से परहेज किया जाता है और अधिक से अधिक सहज, व्यावहारिक और उद्देश्यपरक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप:
कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप कुछ विशिष्ट विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है, जिससे यह सामान्य बोलचाल की हिंदी से अलग होती है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसका स्वरूप स्पष्ट किया जा सकता है:
1. औपचारिकता (Formalism):
कार्यालयीन हिंदी एक औपचारिक भाषा होती है। इसका प्रयोग निर्देश, आदेश, अधिसूचना, रिपोर्ट, शासकीय निर्णय आदि में किया जाता है। इसमें भावनात्मकता या व्यक्तिगत शैली की बजाय निस्पृह और वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति प्रमुख होती है।
2. सरलता और स्पष्टता:
कार्यालयीन भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। वाक्य छोटे, स्पष्ट और सटीक होने चाहिए ताकि पाठक को समझने में कठिनाई न हो। उदाहरणतः, “आपसे अनुरोध है कि निर्धारित तिथि से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करें।” – यह वाक्य संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्यपरक है।
3. प्रमाणिक शब्दावली का प्रयोग:
कार्यालयीन हिंदी में टकसाली (शुद्ध और मानक) हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथासंभव संस्कृतनिष्ठ लेकिन प्रचलित शब्दों को प्राथमिकता दी जाती है। परंतु, अति कठिन शब्दों से परहेज किया जाता है।
4. प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली:
प्रत्येक विभाग की अपनी तकनीकी शब्दावली होती है। कार्यालयीन हिंदी में उन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो राजभाषा विभाग द्वारा मान्य और अधिकृत किए गए हों, जैसे कि “minutes” के लिए “कार्यवृत्त”, “circular” के लिए “परिपत्र” आदि।
5. वस्तुनिष्ठ और निर्देशात्मक भाषा:
कार्यालयीन हिंदी में तथ्यों को बिना किसी पक्षपात के प्रस्तुत किया जाता है। आदेशात्मक, निर्देशात्मक और निर्णयात्मक शैली का प्रयोग होता है। उदाहरण: “उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।”
6. प्रारूपिकता (Format-based writing):
हर प्रकार के पत्र, सूचना, अधिसूचना, आदेश आदि के लिए निश्चित प्रारूप निर्धारित होते हैं। कार्यालयीन हिंदी में इन प्रारूपों का पालन अनिवार्य होता है।
कार्यालयीन हिंदी के उद्देश्य:
कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग केवल भाषा के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य भी हैं। प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1. राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकरूपता:
हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। कार्यालयीन हिंदी के प्रयोग से देश के विभिन्न भागों में एक भाषाई समानता बनी रहती है जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।
2. राजभाषा नीति का अनुपालन:
भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी को केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज की भाषा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत कार्यालयों को हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. सरकारी संचार में पारदर्शिता और जनता से जुड़ाव:
सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से आम जनता को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझना सरल होता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और प्रशासन आम जन से अधिक जुड़ाव अनुभव करता है।
4. कार्यकुशलता और समय की बचत:
एक समान और स्पष्ट भाषा में कार्य करने से कार्यालयों में त्रुटियाँ कम होती हैं, संवाद प्रभावी होता है और कार्य निष्पादन में समय की बचत होती है।
5. भाषाई सशक्तिकरण:
कार्यालयीन हिंदी के प्रयोग से हिंदी भाषा के व्यावसायिक एवं प्रशासनिक पक्ष का विकास होता है। इससे हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहकर आधुनिक, तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों की समर्थ भाषा बनती है।
कार्यालयीन हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र:
कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे:
- फाइलों पर टिप्पणियाँ और नोट लिखना
- शासकीय पत्राचार
- परिपत्र, अधिसूचना, आदेश, निर्देश आदि जारी करना
- वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, तात्कालिक सूचना लिखना
- बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना
- अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिंदी में)
- ई-कार्यालय प्रणाली में हिंदी का प्रयोग
- राजभाषा प्रगति रिपोर्ट तैयार करना
कार्यालयीन हिंदी को प्रोत्साहित करने के प्रयास:
भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी को कार्यालयों में प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जाती हैं, जैसे:
- राजभाषा विभाग की स्थापना: यह विभाग केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की निगरानी करता है।
- हिंदी कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण: कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस: हर साल 14 सितंबर को ‘हिंदी दिवस’ मनाया जाता है तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं।
- हिंदी में प्रोत्साहन पुरस्कार: जो कार्यालय अथवा कर्मचारी अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं, उन्हें राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
- राजभाषा समिति की बैठकें: इन बैठकों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती है।
कार्यालयीन हिंदी की चुनौतियाँ:
हालाँकि कार्यालयीन हिंदी को प्रोत्साहित करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इसके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
- तकनीकी शब्दावली का अभाव: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विधि आदि क्षेत्रों की सटीक पारिभाषिक शब्दावली हिंदी में सीमित है।
- कर्मचारियों की प्रशिक्षण में कमी: कई कर्मचारी कार्यालयीन हिंदी में दक्ष नहीं होते, जिससे अंग्रेजी पर निर्भरता बनी रहती है।
- मन की अनिच्छा: कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी को कमतर मानते हैं और अंग्रेजी को ही श्रेष्ठ समझते हैं।
- डिजिटल संसाधनों की कमी: कार्यालयों में हिंदी टाइपिंग सुविधाओं, सॉफ्टवेयर आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती।
उपसंहार:
कार्यालयीन हिंदी भारतीय प्रशासन की आत्मा है। यह न केवल एक कार्यशील भाषा है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और भाषाई गौरव की पहचान भी है। यदि इसे सही दिशा में और सतत प्रयासों द्वारा विकसित किया जाए तो यह प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और समानता लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
हिंदी को कार्यालयों में केवल एक “दायित्व” न समझकर, “साधन” और “संपर्क का माध्यम” माना जाना चाहिए। इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने से न केवल हिंदी का विकास होगा, बल्कि भारत की भाषाई अस्मिता और प्रशासनिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।