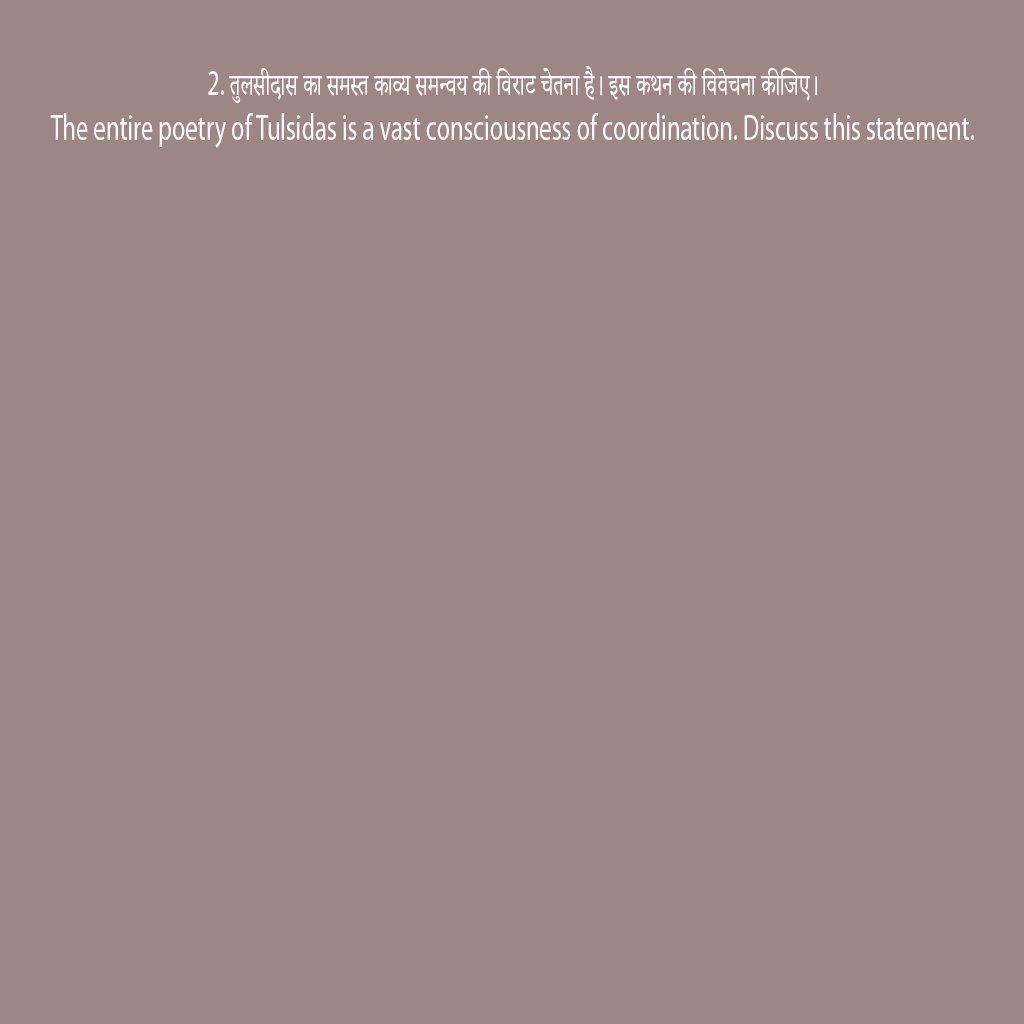तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेतना है। इस कथन की विवेचना कीजिए।Vidyapati’s contribution in the tradition of lyric poetry
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
भूमिका
भारतीय साहित्य और संस्कृति के इतिहास में तुलसीदास एक ऐसे युगद्रष्टा कवि के रूप में स्थापित हैं, जिनका समस्त काव्य समन्वय की भावना से ओत-प्रोत है। तुलसीदास न केवल हिंदी के महान कवि हैं, बल्कि एक संत, दार्शनिक, समाज-सुधारक और भारतीय अध्यात्म के संवाहक भी हैं। उनके काव्य में भक्ति, नीति, दर्शन, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति और मानवता की व्यापक झलक मिलती है।
तुलसीदास ने अपने युग की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विविधताओं को समन्वित करके एक ऐसा काव्य-संसार रचा जिसमें सभी धाराएँ मिलती हैं और किसी प्रकार का टकराव नहीं होता। यही कारण है कि आलोचक कहते हैं – “तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेतना है।”
तुलसीदास का युग संदर्भ
तुलसीदास का जीवनकाल 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आता है। यह वह समय था जब भारतीय समाज अनेक संकटों से जूझ रहा था:
- राजनीतिक अस्थिरता (मुगल शासन),
- सांप्रदायिक संघर्ष,
- जातीय विषमता,
- धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड,
- समाज में स्त्री और निम्नवर्ग की उपेक्षा,
- संस्कृत और ब्रज भाषा में विभाजन।
ऐसे समय में तुलसीदास ने अपने काव्य में ऐसी चेतना का विकास किया जिसमें भक्ति और मानवता का समन्वय, धर्म और नैतिकता की पुनर्परिभाषा, सामाजिक समरसता, और विभिन्न विचारधाराओं का समावेश था।
समन्वय की अवधारणा
‘समन्वय’ का अर्थ है विभिन्न विरोधी या भिन्न विचारों, भावनाओं, या तत्त्वों को एक ऐसी समरस प्रणाली में ढालना जहाँ उनका मूल अस्तित्व सुरक्षित रहे परंतु एकता और सामंजस्य भी बना रहे।
तुलसीदास ने इस समन्वय को न केवल विचारधारा में, बल्कि भाषा, शैली, पात्र, दर्शन, धर्म, और काव्यशास्त्र के स्तर पर भी प्रस्तुत किया।
1. धार्मिक समन्वय
तुलसीदास का काव्य धार्मिक समन्वय की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने भक्ति को संप्रदाय के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसे व्यापक और सार्वभौमिक रूप प्रदान किया।
(क) शैव और वैष्णव का समन्वय
तुलसीदास स्वयं विष्णु (राम) भक्त थे, परंतु उन्होंने शिव को भी समान श्रद्धा के साथ स्थान दिया। वे कहते हैं:
“सिव द्रोही मम दास कहावा। सो नर मोहि सपनेहुँ न भावा॥”
(रामचरितमानस)
यहाँ स्पष्ट है कि तुलसीदास के लिए रामभक्ति में शिवभक्ति का विरोध नहीं, बल्कि पूरक स्थान है। राम और शिव दोनों की एकता तुलसी के समन्वय दृष्टिकोण को दर्शाती है।
(ख) सगुण और निर्गुण भक्ति का समन्वय
तुलसीदास ने ‘सगुण भक्ति’ का प्रचार किया, लेकिन उन्होंने ‘निर्गुण’ के दर्शन को भी नकारा नहीं। वे राम को साकार रूप में पूजते हैं, परंतु राम के परम तत्व को ‘निर्गुण ब्रह्म’ के रूप में भी स्वीकार करते हैं।
“ब्रम्ह अनामय अज अभिनाशी। सत चित अनंद स्वरूप अविनाशी॥”
यह दर्शाता है कि वे सगुण-निर्गुण की बहस से ऊपर उठकर भक्ति के मूल तत्व को प्राथमिकता देते हैं।
2. सामाजिक समन्वय
तुलसीदास का काव्य तत्कालीन समाज की विषमताओं और भेदभाव के विरुद्ध समरसता का संदेश देता है।
(क) जाति-पाति का विरोध
रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, जाति-पाति का कोई महत्व नहीं है:
“जाति-पाँति पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई।”
तुलसीदास की यह पंक्ति सामाजिक समरसता का उद्घोष है।
(ख) स्त्री और शूद्रों के प्रति सहानुभूति
यद्यपि तुलसी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों को निम्न स्थान दिया, परंतु यदि पूरे काव्य का गहन अध्ययन किया जाए, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने तुलसीयुगीन समाज की सीमाओं में रहते हुए भी नारी की गरिमा और शूद्रों की भक्ति को सम्मान दिया।
“भक्तन सो मोहि प्रीति अधिकाई। बिनु सेवा न पावहि भलाई॥”
यह कथन किसी भी जाति, वर्ग, लिंग को सीमित नहीं करता, बल्कि सेवाभाव और भक्ति को सर्वोच्च मानता है।
3. भाषिक समन्वय
तुलसीदास का सबसे बड़ा काव्यिक योगदान यह है कि उन्होंने भाषा को संस्कृत की सीमा से निकालकर जनभाषा में साहित्य का निर्माण किया।
(क) अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग
रामचरितमानस अवधी में है, तो विनय पत्रिका और कवितावली ब्रजभाषा में। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत और लोकभाषाओं का भी प्रयोग किया। इस प्रकार उन्होंने भाषिक एकता और जनभाषा के माध्यम से ज्ञान का democratization किया।
(ख) लोक और शास्त्र का समन्वय
तुलसी के काव्य में जहाँ एक ओर शास्त्रीय परंपरा के गूढ़ तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर लोकमानस, लोकगीत, परंपराएँ, हास्य, व्यंग्य और कहावतें भी समाहित हैं।
उदाहरण:
“सियाराम मय सब जग जानी।
करहु प्रणाम जोरि जुग पानी॥”
यह शास्त्र और लोक की ऐसी सुंदर संगति है जो हर स्तर के पाठक को प्रभावित करती है।
4. साहित्यिक समन्वय
तुलसीदास ने विविध काव्य परंपराओं को अपने काव्य में समाहित किया:
(क) रचना विधाओं का समन्वय
- रामचरितमानस – महाकाव्य परंपरा
- कवितावली – वीर रस प्रधान
- विनय पत्रिका – भक्ति और करुण रस का सामंजस्य
- हनुमान चालीसा – स्तोत्र शैली में
उनकी काव्य रचनाओं में शृंगार, वीर, भक्ति, करुण, और शांत रसों का समन्वय मिलता है।
(ख) कथा और दर्शन का समन्वय
रामचरितमानस एक कथा है, लेकिन यह केवल कथा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक ग्रंथ भी है। इसमें राम की कथा के माध्यम से धर्म, नीति, कर्म, ज्ञान, और भक्ति का गूढ़ तत्त्व समाहित है।
5. आध्यात्मिक समन्वय
तुलसीदास का आध्यात्मिक चिंतन अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत दर्शन का समन्वय करता है।
- उन्होंने राम को साकार ईश्वर के रूप में चित्रित किया, जो भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं।
- उनके राम वेदों से प्रमाणित, नीति और मर्यादा के रक्षक, और भक्तों के संरक्षक हैं।
इस प्रकार उनका आध्यात्मिक चिंतन न तो केवल ज्ञानमार्ग है, न केवल कर्म, और न केवल भक्ति – बल्कि यह सभी का समन्वय है।
6. मानवता और नैतिकता का समन्वय
तुलसीदास का काव्य केवल धार्मिक नहीं, मानवीय भी है। उन्होंने मानव जीवन की समस्याओं को समझते हुए धर्म का ऐसा व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया जिसमें नीति और करुणा दोनों का समावेश है।
(क) आदर्श नायक – श्रीराम
राम न केवल ईश्वर हैं, बल्कि एक आदर्श राजा, पुत्र, पति, भाई, और मनुष्य हैं। उनके माध्यम से तुलसी ने सामाजिक और नैतिक आदर्शों को स्थापित किया।
“राम राज बैठें त्रैलोका।
हरषित भये गए सब शोका॥”
यह रामराज्य की कल्पना एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रतीक है।
7. राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय
तुलसीदास का काव्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक छवियों को समाहित करता है। रामचरितमानस में अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, लंका, चित्रकूट जैसे अनेक स्थलों का चित्रण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुलसीदास का काव्य एक सांस्कृतिक सेतु है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है।
8. तुलसीदास की समन्वय चेतना: समकालीनों के संदर्भ में
तुलसीदास के समकालीन कबीर, सूरदास, रैदास, और मीरा भक्ति के अन्य रूपों के प्रवर्तक थे। तुलसीदास ने उनके विचारों से सहमति-असहमति के बावजूद अपने काव्य में समन्वय का मार्ग चुना:
- कबीर की निर्गुण भक्ति
- मीरा की माधुर्य भक्ति
- सूर की वात्सल्य भक्ति
इन सबके तत्त्व तुलसीदास के काव्य में संयोजित हैं।
निष्कर्ष
“तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेतना है”—यह कथन न केवल सत्य है, बल्कि तुलसी साहित्य का सार भी है। उन्होंने धर्म, दर्शन, समाज, भाषा, साहित्य, राजनीति और संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों में समन्वय का जो विराट चित्र खींचा, वह उन्हें केवल कवि ही नहीं, अपितु युगद्रष्टा, समाज सुधारक, और सांस्कृतिक शिल्पी बना देता है।
उनका समन्वय:
- शिव और विष्णु का,
- सगुण और निर्गुण का,
- नारी और पुरुष का,
- शूद्र और ब्राह्मण का,
- संस्कृत और लोकभाषा का,
- भक्ति और नीति का,
- ज्ञान और भाव का,
- कथा और दर्शन का—
एक ऐसा विराट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो आज भी भारतीयता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है।
इसलिए तुलसीदास का काव्य केवल साहित्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की विराट चेतना का दर्पण है।