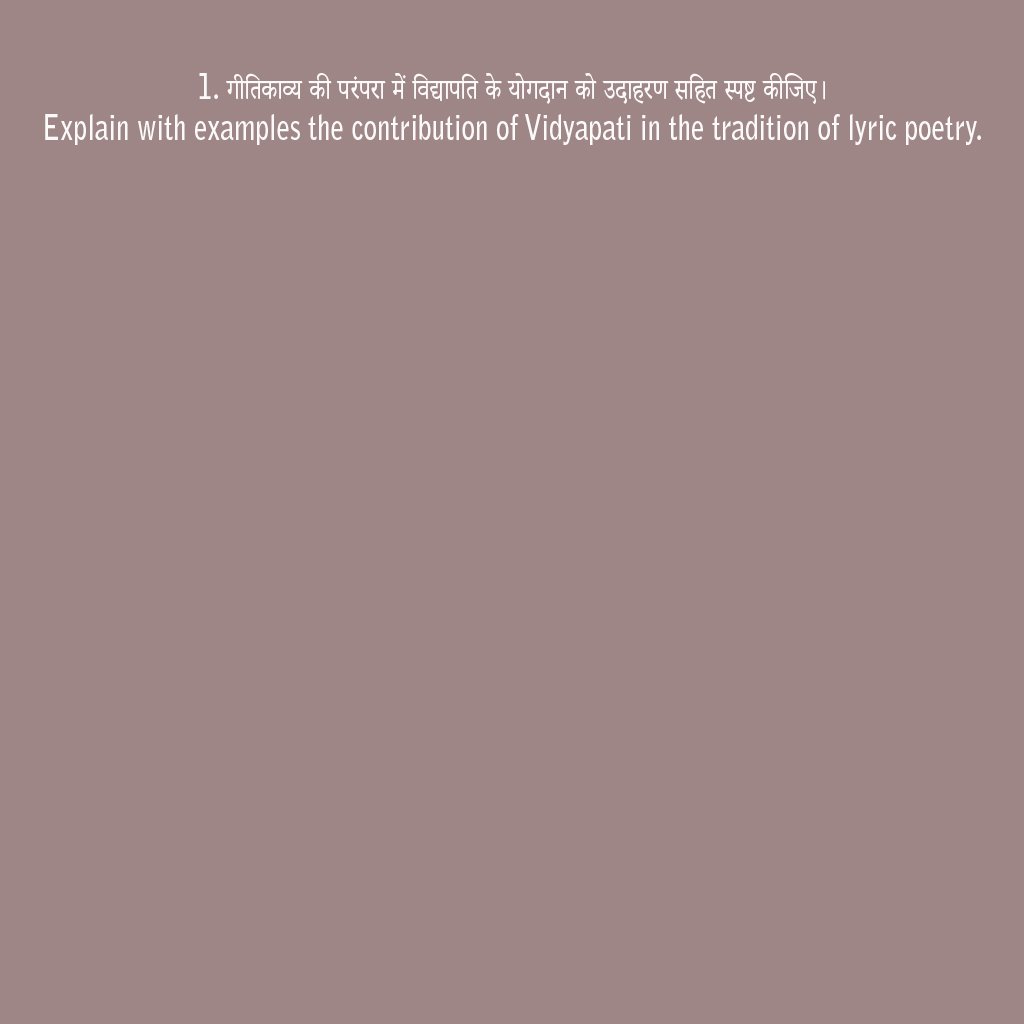गीतिकाव्य की परंपरा में विद्यापति का योगदान Vidyapati’s contribution in the tradition of lyric poetry
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
भूमिका:
भारतीय काव्य परंपरा में गीति काव्य (लिरिक काव्य) का एक विशिष्ट स्थान रहा है। गीति काव्य वह काव्य होता है जिसमें भावना की प्रधानता होती है और जो संगीत के साथ गाया जा सकता है। इसमें कवि की निजी अनुभूतियाँ, प्रेम, भक्ति, सौंदर्य और रसानुभूति का स्वरूप अधिक होता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को गीति काव्य का स्वर्णकाल माना जाता है, और इस परंपरा को समृद्ध बनाने में अनेक कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कवियों में विद्यापति का नाम सर्वोपरि है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में जिस कोमलता और सौंदर्य के साथ प्रेम और भक्ति को गीतिकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया, वह उन्हें इस परंपरा का एक अमर स्तंभ बना देता है।
विद्यापति: संक्षिप्त परिचय
विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी में मिथिला (वर्तमान बिहार राज्य) के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गणपति ठाकुर एक विद्वान व्यक्ति थे। विद्यापति काव्य, संगीत, राजनीति, धर्म और साहित्य के विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। उन्हें “मैथिल कोकिल” की उपाधि दी गई, जो उनकी काव्यात्मक मधुरता और भावनात्मकता को दर्शाती है।
विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा के प्रकांड विद्वान थे, परंतु उनकी पहचान मुख्य रूप से मैथिली के गीतिकवि के रूप में हुई। उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। विशेष रूप से राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन उनके गीतिकाव्य की आत्मा है।
गीतिकाव्य की परंपरा में विद्यापति का स्थान
1. गीतिकाव्य की परंपरा का विकास
गीतिकाव्य की परंपरा की जड़ें संस्कृत साहित्य के संघ काव्य, प्राकृत गीतिकाव्य, अपभ्रंश, और लोकगीतों में देखी जा सकती हैं। कालिदास, अमरु और भास जैसे कवियों ने संस्कृत में गीति-रस की प्रधानता वाले काव्य रचे। लेकिन यह परंपरा अपभ्रंश और फिर लोकभाषाओं में अधिक सशक्त रूप में फली-फूली।
विद्यापति उस परंपरा से जुड़ते हैं जिसमें प्रेम की अनुभूति, स्त्री की संवेदना, और निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति को केंद्र में रखा गया। उन्होंने नारी मन की कोमलतम भावनाओं को सहज भाषा और मधुर संगीतात्मक शैली में व्यक्त किया, जो गीतिकाव्य की प्रमुख विशेषता है।
2. विद्यापति की काव्यगत विशेषताएँ और गीतिकाव्य के प्रति योगदान
(क) प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति
विद्यापति के गीतों में राधा और कृष्ण के प्रेम की मधुरता, विरह की वेदना, मिलन का उल्लास, और नायिका की अंतरंग भावनाओं का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण है। उन्होंने राधा के मनोविज्ञान को इस गहराई से अभिव्यक्त किया कि उनकी कविता स्त्री संवेदना की प्रतीक बन गई।
उदाहरण:
“जालि जनि गोसाइं!
आन हाथ उठैबे नाहिं।
हेरि मुंह मोर कटि पटि तोहि बाँधब,
अधर मूँदि करब चुम्बन चाहिं…”
इस गीत में राधा की चंचलता, लज्जा और प्रेम की तीव्रता, नायक के प्रति प्रबल आकर्षण और मिलन की उत्कंठा अत्यंत कोमलता से चित्रित है।
(ख) लोक भाषा और शैली का प्रयोग
विद्यापति ने मैथिली भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। उन्होंने मैथिली को इतना मधुर और रसपूर्ण बना दिया कि वह भक्ति और श्रृंगार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की भाषा बन गई। उनकी भाषा सरल, संगीतमय और स्वाभाविक थी, जिससे उनकी रचनाएँ जनमानस में लोकप्रिय हो गईं।
उनकी भाषा में लोकगीतों की मिठास, लोक व्यवहार की सहजता, और संगीत की रसनिष्ठता मिलती है। इस कारण उनके गीतों को गाया भी गया, और शास्त्रीय संगीत में भी स्थान मिला।
(ग) नारी मन की सजीव अभिव्यक्ति
विद्यापति के गीतों में नारी मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएँ बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त हुई हैं। चाहे राधा की विरह व्यथा हो या मिलन की संकोच भरी खुशी, सब कुछ बहुत जीवंत और संवेदनशील रूप में वर्णित है।
उदाहरण:
“रुनु झुनु बाजे पैंजनिया,
राधिके चरन धरे…”
इस गीत में नायिका के चलने की मधुर ध्वनि, उसकी चाल, उसका लजाना, और मिलन की छवि अत्यंत स्वाभाविक रूप में उभरती है।
(घ) भक्ति और श्रृंगार का समन्वय
विद्यापति का काव्य इस दृष्टि से विशेष है कि उसमें संयोग और वियोग की श्रृंगारिक भावनाओं में भक्ति का रस भी समाहित है। उनके राधा-कृष्ण गीतों में प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का संकेत मिलता है। यह परंपरा आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु, मीरा, और सूरदास में फली-फूली।
कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, जो माधुर्य भक्ति का मूल दर्शन है।
3. विद्यापति और गीतिकाव्य की ध्वनि-संरचना
विद्यापति की रचनाओं में ध्वनि योजना इतनी मधुर और संगत होती है कि उनकी रचनाएँ पढ़ने की अपेक्षा सुनने और गाने में अधिक प्रभावशाली लगती हैं। उन्होंने पद्य की तालबद्धता, लय, तुकबंदी और अनुप्रास का अत्यंत कुशल प्रयोग किया।
उदाहरण:
“पिया मोरे! पिया मोरे!
मोरी सुधि नाहिं लेहु रे!”
यहाँ “पिया मोरे” की पुनरावृत्ति से व्याकुलता और भावों की तीव्रता प्रकट होती है, जो गीति-काव्य का मूल गुण है।
4. विद्यापति की रचनाओं में सांस्कृतिक छवियाँ
विद्यापति के गीतों में मिथिला क्षेत्र की संस्कृति, वस्त्र, गहने, प्रकृति, त्योहार, और लोकाचार का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने ऋतु वर्णन, सांझ-सवेरा, नदी, पवन, और प्रकृति के सौंदर्य को प्रेम के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया।
उदाहरण:
“नदी किनारे बसी राधा,
हेरि-हेरि जमुना जल…”
यहाँ राधा का सौंदर्य और प्राकृतिक परिवेश, दोनों प्रेम की भावना को गहराई से दर्शाते हैं।
5. गीतिकाव्य पर विद्यापति के प्रभाव का प्रसार
विद्यापति का प्रभाव न केवल मैथिली साहित्य तक सीमित रहा, बल्कि:
- बंगाल, अवध, ब्रज, और राजस्थानी साहित्य में भी उनकी शैली का अनुसरण हुआ।
- चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बंगाल में विद्यापति के पदों को भक्ति गीतों की तरह गाते थे।
- रसखान, सूरदास, मीरा आदि ने राधा-कृष्ण प्रेम का जो चित्रण किया, उस पर विद्यापति की छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
- रवींद्रनाथ टैगोर और विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय जैसे आधुनिक बंगाली साहित्यकारों ने भी विद्यापति के गीतों को सराहा और उनके अनुवाद किए।
6. गीतिकाव्य के विकास में विद्यापति की प्रासंगिकता
आज भी विद्यापति के गीत:
- शास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, और कजरी के रूप में गाए जाते हैं।
- सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में उनकी रचनाएँ विशेष रूप से प्रस्तुत की जाती हैं।
- उनकी कविता कालजयी है क्योंकि उसमें मानवीय संवेदना, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संयोग मिलता है।
निष्कर्ष
गीतिकाव्य की परंपरा में विद्यापति का योगदान अविस्मरणीय और अनुपम है। उन्होंने मैथिली भाषा में गीतिकाव्य को नया जीवन दिया, और प्रेम व भक्ति के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज को भी एक गहन भावनात्मक धारा प्रदान की। उनके गीतों में नारी मन की संवेदना, प्रकृति का सौंदर्य, और प्रेम की मधुरता इतनी स्वाभाविकता और भावुकता से प्रकट होती है कि वे आज भी उतने ही जीवंत और आकर्षक लगते हैं।
विद्यापति न केवल एक कवि थे, बल्कि मानव मन के कुशल चितेरे, संगीत के आचार्य, और प्रेम-भक्ति के पुरोधा भी थे। उनके गीतिकाव्य में जो रस, लय, और सौंदर्य है, वह उन्हें हिंदी तथा भारतीय साहित्य के गीतिकाव्य परंपरा में एक अमर स्थान प्रदान करता है।