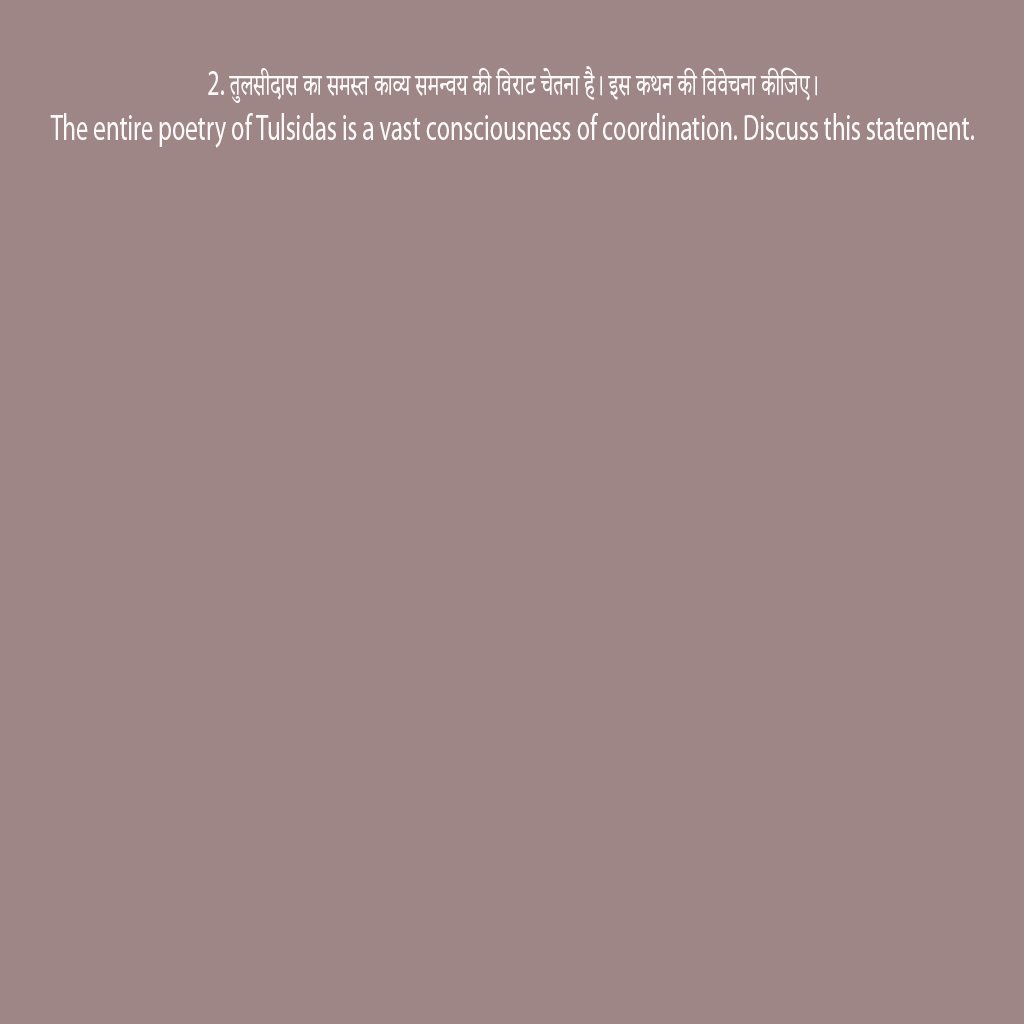तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेतना है। इस कथन की विवेचना कीजिए। The entire poetry of Tulsidas is a vast consciousness of coordination. Discuss this statement.
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
भूमिका
भारतीय काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान अत्यंत विशिष्ट और गौरवपूर्ण है। उन्होंने न केवल भक्ति काव्यधारा को समृद्ध किया, अपितु अपनी काव्यशैली, भाषा, और वैचारिक दृष्टिकोण से जनमानस को एकजुट कर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की जड़ों को गहराई दी। तुलसीदास का समस्त काव्य केवल धार्मिक भक्ति या रामकथा का वर्णन नहीं है, वरन् वह समन्वय की ऐसी विराट चेतना है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, वेद, पुराण, उपनिषद, लोकमंगल, नीति, समाज सुधार, मानवता और संस्कृतियों का अद्वितीय संगम दिखाई देता है।
तुलसीदास ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक धाराओं को अपने काव्य में इस प्रकार समाहित किया कि वह न केवल उस समय की विभाजित चेतनाओं को जोड़ सका, बल्कि आज भी समाज को एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक आत्मबोध की प्रेरणा देता है।
तुलसीकाव्य में समन्वय की अवधारणा
“समन्वय” का अर्थ होता है विभिन्न विचारों, तत्वों या धाराओं के मध्य संतुलन और एकरूपता की स्थापना। तुलसीदास के काव्य की मूल चेतना यही है—विरोधों का सामंजस्य, भिन्न-भिन्न मतों का एकीकरण, और एक ऐसी चेतना का निर्माण जो सभी के लिए ग्राह्य और प्रेरणादायक हो।
तुलसीदास ने किसी एक दर्शन, पंथ या वर्ग विशेष का समर्थन न कर संपूर्ण भारतीय परंपरा का ऐसा समुच्चय प्रस्तुत किया जिसमें सबके लिए स्थान है। यही कारण है कि उनका काव्य समन्वय की विराट चेतना का प्रतीक माना जाता है।
1. भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय
भारतीय दर्शन की तीन प्रमुख धाराएँ—भक्ति, ज्ञान, और कर्म—तुलसीकाव्य में परस्पर पूरक रूप में विद्यमान हैं।
- भक्ति: तुलसीदास मूलतः भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ‘रामचरितमानस’ में भक्ति की सर्वोपरिता प्रतिपादित की गई है—
“भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी।।” - ज्ञान: तुलसीदास केवल भावुक भक्त नहीं, वे उच्चकोटि के ज्ञानी भी हैं। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत के तत्वों को जनभाषा में प्रस्तुत किया।
“ज्ञान खगेस समुझि मन माहीं। हरष बिसाद बिमोह नसाहीं।।” - कर्म: तुलसीदास के काव्य में निष्काम कर्मयोग का भी समर्थन मिलता है। उन्होंने राम को ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ के रूप में प्रस्तुत कर कर्म का आदर्श रूप चित्रित किया।
तुलसी ने इन तीनों धाराओं को इस प्रकार जोड़ा कि कोई भी एकांगी न रहे, और सभी एक दूसरे के पूरक बनें। यह समन्वय उस काल में विशेष महत्वपूर्ण था जब संप्रदायवाद और दार्शनिक विभाजन चरम पर था।
2. सांस्कृतिक समन्वय
तुलसीदास का युग सांस्कृतिक संकटों का युग था। मध्यकाल में जब भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, धर्म-संस्कृति खतरे में थी, तब तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे काव्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की रक्षा की।
- उन्होंने संस्कृत की गूढ़ता को जनभाषा में उतारा (अवधी, ब्रज, आदि)।
- रामकथा के माध्यम से वैदिक, पुराणिक, लोक, और तांत्रिक संस्कृतियों को एक सूत्र में बाँधा।
- उनके काव्य में वर्णाश्रम धर्म का भी संतुलित चित्रण मिलता है—जहाँ हर वर्ग के लिए धर्म पालन का अलग महत्व है।
इस प्रकार तुलसीकाव्य ने संस्कृत, अपभ्रंश, लोककथा, पुराण, तथा धर्मशास्त्रों के तत्वों का समन्वय करते हुए एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना का निर्माण किया जो आज भी जनमानस में जीवित है।
3. धार्मिक समन्वय
तुलसीदास के समय में भारत में धार्मिक मतभेद प्रबल हो गए थे—शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों के बीच संघर्ष था। तुलसीदास ने ‘राम’ के माध्यम से एक ऐसे आराध्य की स्थापना की जो सबके लिए था:
- उन्होंने राम को ब्रह्म का अवतार बताया, लेकिन उन्हें मानव रूप में ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ के रूप में प्रतिष्ठित किया।
- रामचरितमानस में शिव और राम का संबंध पारस्परिक श्रद्धा पर आधारित है—
“गिरिजा यह प्रसंग सुनि, मनवा हरषित होय।” - तुलसीदास ने कभी किसी मत या धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि सभी मतों की श्रेष्ठ बातों को अपनाया।
उनका यह दृष्टिकोण उस समय के कट्टर धार्मिक संघर्षों के मध्य समन्वय की एक मधुर वाणी के समान था।
4. लोक और शास्त्र का समन्वय
तुलसीदास ने एक ओर वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन आदि शास्त्रीय ज्ञान का सहारा लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने लोकमानस की भावनाओं को भी महत्व दिया।
- तुलसी के रामचरितमानस में विद्वानों के लिए शास्त्रार्थ है, तो ग्रामीणों के लिए सरल कथा भी।
- लोकगाथाओं, मुहावरों, कहावतों, रीति-रिवाजों और लोकभाषा को भी उन्होंने सम्मान दिया।
- उन्होंने रामकथा को शास्त्र से निकाल कर जन-जन तक पहुँचाया।
यह लोक-शास्त्र समन्वय ही तुलसीकाव्य को जनमानस में इतना लोकप्रिय बनाता है।
5. भाषा का समन्वय
तुलसीदास ने काव्य में अवधी, ब्रज, संध्या भाषा, और संस्कृत—इन सभी का प्रयोग किया।
- रामचरितमानस अवधी में है, जिसे जनभाषा कहा जाता है।
- विनयपत्रिका में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें कृष्णभक्ति की झलक भी दिखती है।
- उन्होंने संस्कृत के गूढ़ शब्दों को जनभाषा में पिरोया।
उनकी भाषा का यह समन्वय उन्हें सभी वर्गों के लिए ग्राह्य बनाता है—पंडित, ग्रामीण, साधु, गृहस्थ सभी के लिए।
6. नैतिक और सामाजिक समन्वय
तुलसीकाव्य केवल धार्मिक नहीं है, उसमें गहरी सामाजिक चेतना भी है:
- नारी के प्रति सम्मान, परिवार की मर्यादा, शील, सेवा, त्याग जैसे गुणों को उन्होंने प्रतिष्ठा दी।
- शबरी, निषाद, वनवासी—सभी को राम के समीपस्थ बना कर उन्होंने सामाजिक समरसता को बल दिया।
- जाति-पाति, वर्णभेद, अहंकार, पाखंड जैसे सामाजिक दोषों की आलोचना की—
“जाति पाँछाँ पूछिए, जानिए धर्म न हेत।”
“कर्महीन नर पावहि न भव निधि।”
यह सामाजिक समन्वय आज भी तुलसीदास को प्रासंगिक बनाता है।
7. स्त्री-पुरुष, भाव-बुद्धि, और अन्य द्वंद्वों का समन्वय
तुलसीदास ने नारी को सम्मान देते हुए उसका पारंपरिक चित्रण किया, पर उसे केवल कामना की वस्तु नहीं माना। सीता को शक्ति और सहधर्मिणी के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भाव और बुद्धि, श्रद्धा और विवेक—इन द्वंद्वों का संतुलन अपने काव्य में साधा।
- राम स्वयं भावप्रधान हैं, लक्ष्मण बुद्धिप्रधान—दोनों मिलकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- तुलसी की भक्ति केवल भावुकता नहीं, उसमें विवेक और नीति का संगम है।
8. तुलसीकाव्य: भारतीय एकता का प्रतीक
तुलसीदास का काव्य एक ऐसी चेतना का वाहक है, जिसमें भारत की विविधता में एकता की भावना परिलक्षित होती है:
- उत्तर भारत से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक रामचरितमानस की कथा एकजुट करती है।
- विभिन्न बोलियों, रीति-नीति, परंपराओं, धर्मों, जातियों के लोगों को एक सूत्र में बाँधने की सामर्थ्य है तुलसीकाव्य में।
- तुलसीदास ने ‘रामराज्य’ की परिकल्पना दी जो न्याय, शांति और समरसता पर आधारित है—
“दुख हीन, सुख संपन, नगर कोउ न दुखी न दीना।”
उपसंहार
तुलसीदास का समस्त काव्य वास्तव में समन्वय की विराट चेतना है। उन्होंने विरोधों का विरोध नहीं किया, वरन् उन्हें सहेज कर सामंजस्य की भावना से एकीकृत किया। उनका काव्य भारतीय जीवन-दर्शन, समाज, संस्कृति, और धर्म का एक ऐसा दर्पण है जिसमें समन्वय ही मूल तत्व है। इसीलिए वे केवल कवि नहीं, एक युगद्रष्टा, समाज-सुधारक और भारतीय एकता के सूत्रधार माने जाते हैं।
तुलसीकाव्य आज भी हमें यह संदेश देता है कि विविधता में एकता संभव है, और परस्पर विरोधों में भी समरसता उत्पन्न की जा सकती है—बस आवश्यकता है दृष्टिकोण की, जैसे तुलसीदास ने अपनाया।
अतः यह कहना पूर्णतः उचित है कि “तुलसीदास का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेतना है।”