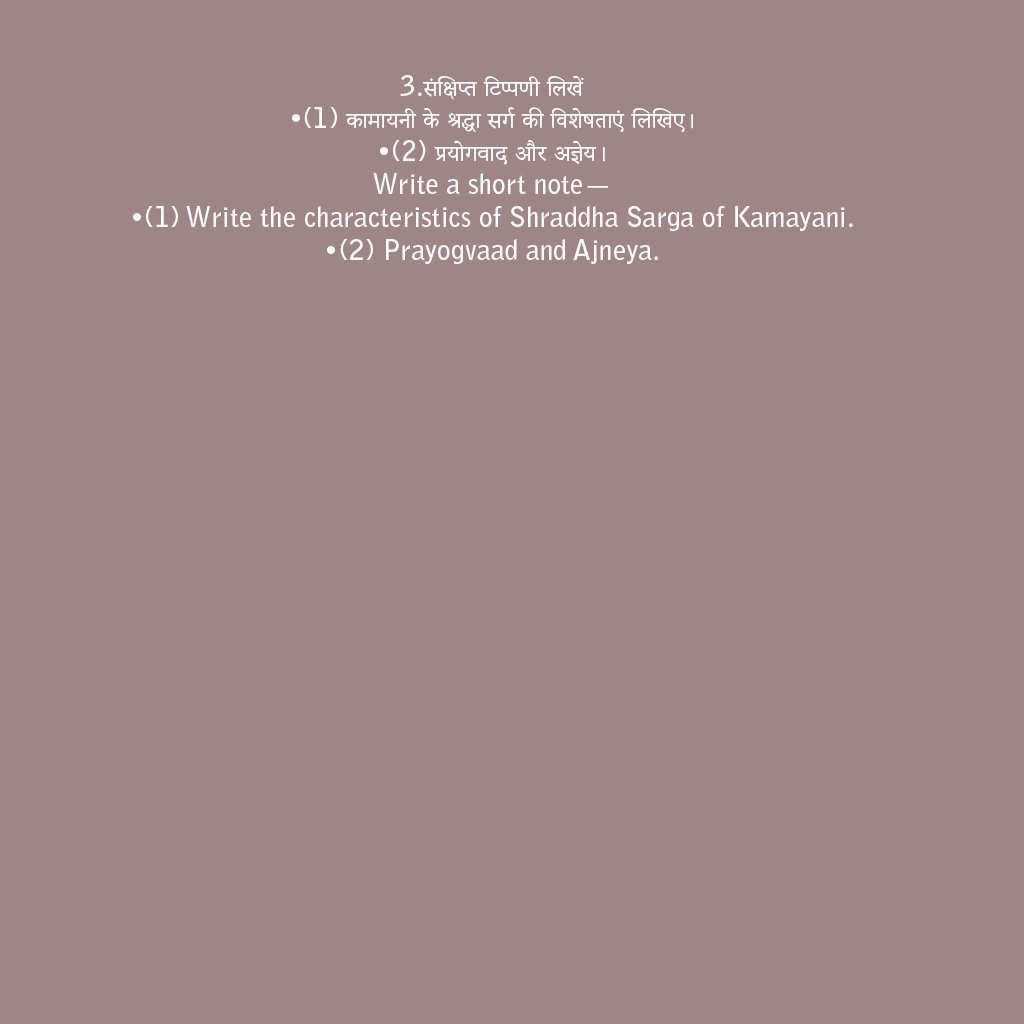कामायनी के श्रद्धा सर्ग प्रयोगवाद और अज्ञेय Kamayani’s Shraddha Sarga Experimentalism and Ajneya
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें
•(1) कामायनी के श्रद्धा सर्ग की विशेषताएं लिखिए।
•(2) प्रयोगवाद और अज्ञेय।
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
(1) कामायनी के श्रद्धा सर्ग की विशेषताएँ
कामायनी (1936) जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील-मननशील काव्य है। यह छंदबद्ध महाकाव्य मानव मन के विभिन्न भावों और चिंतन-स्तरों को व्यक्त करता है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की रचना इस काव्य के आधार-स्तंभ के रूप में हुई है, जिसमें श्रद्धा को प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, स्त्रीत्व और भावनात्मक उन्नयन की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्य विशेषताएँ:
1. श्रद्धा का प्रतीकात्मक स्वरूप
श्रद्धा यहाँ केवल एक स्त्री पात्र नहीं, बल्कि वह मानसिक अवस्था है जो मनुष्य के जीवन को स्थिर, आश्वस्त और आध्यात्मिक बनाती है। वह अज्ञेय और विज्ञान की प्रतीक ‘इड़ा’ की तुलना में अधिक कोमल और आध्यात्मिक है।
2. आदिकालीन पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक संवेदना
श्रद्धा सर्ग में आदिकालीन वातावरण को आधार बनाकर लेखक ने मानव मन की मूल प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया है — विशेषतः प्रेम, करुणा, आत्मसमर्पण और विश्वास को।
3. मानव मन की द्वंद्वात्मकता का आरंभ
श्रद्धा सर्ग से ही कामायनी के मुख्य द्वंद्व का आरंभ होता है — श्रद्धा बनाम इड़ा, अर्थात भावना बनाम बुद्धि। यह द्वंद्व पूरे महाकाव्य में चलता है और मानवता की विकास-यात्रा को चित्रित करता है।
4. प्रकृति और सौंदर्य का सुंदर चित्रण
इस सर्ग में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण अत्यंत काव्यात्मक है। प्रसाद ने जलप्रलय के बाद की शांत प्रकृति और उसमें उत्पन्न श्रद्धा के रूप को दिव्य सौंदर्य से सजाया है।
5. भावात्मक गहराई और दार्शनिकता
श्रद्धा सर्ग में दार्शनिकता और भावात्मक गहराई का सुंदर समन्वय है। यह केवल भाव-विलास नहीं, बल्कि मानव जीवन की दिशा तय करने वाली चेतना है।
6. सौंदर्य और छायावादी प्रभाव
यह सर्ग छायावाद की चरम सीमा का उदाहरण है – कल्पना, रहस्य, सौंदर्य और आत्मानुभूति इसकी विशेषताएँ हैं।
निष्कर्ष
श्रद्धा सर्ग ‘कामायनी’ का मूलाधार है, जो न केवल काव्य की सौंदर्यात्मकता को उन्नत करता है, बल्कि एक दार्शनिक विमर्श की भूमि भी तैयार करता है। यह मानवता के लिए करुणा, निष्ठा और श्रद्धा जैसे मूल्यों की महत्ता को स्पष्ट करता है।
(2) प्रयोगवाद और अज्ञेय
प्रयोगवाद: एक साहित्यिक आंदोलन
प्रयोगवाद हिंदी कविता का वह युग था (मुख्यतः 1943–1954), जब कवियों ने साहित्य को नई दिशा, नया रूप और नया विषय देने की कोशिश की। यह छायावाद के भावुक और रहस्यवादी संसार से बाहर निकलने की क्रांतिकारी पहल थी।
प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएँ:
- व्यक्तिवाद की प्रधानता – कवि अपने अंतर अनुभवों और मानसिक जटिलताओं को अभिव्यक्त करता है।
- नवीन शिल्प और शैली – छंदों से मुक्त होकर, नई भाषा, नए प्रतीक, नए बिंब और नई संवेदनाएं सामने आईं।
- बौद्धिकता और तर्कप्रधानता – अनुभूति के साथ-साथ विचार भी कविता का अंग बने।
- सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों से मुठभेड़ – प्रयोगवादी कविता आधुनिक जीवन की विडंबनाओं, अकेलेपन, अस्तित्व और अनिश्चितता को स्वर देती है।
- काव्य भाषा का वैज्ञानिक और अभिजात प्रयोग – भाषा सटीक, संक्षिप्त और गूढ़ होती है।
अज्ञेय और प्रयोगवाद:
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ को प्रयोगवाद का प्रणेता, संरक्षक और प्रवक्ता माना जाता है। उन्होंने 1943 में ‘तार-सप्तक’ का संपादन किया, जो प्रयोगवाद की घोषणा-पत्र की तरह था।
1. अज्ञेय: प्रयोगवादी चेतना के प्रवर्तक
- अज्ञेय ने छायावादी भावुकता से हटकर कविता को मनुष्य के भीतरी संघर्ष, आत्मसंधान और वैचारिक जटिलताओं से जोड़ा।
- उनके काव्य में आधुनिक मनुष्य की विखंडित चेतना, द्वंद्व और अकेलापन प्रमुख हैं।
- उन्होंने साहित्य को “मुक्त” करने की बात की — न केवल शिल्प और छंदों से, बल्कि विषयों की बंदिशों से भी।
2. तार सप्तक का योगदान
अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तार सप्तक’ (1943) सात कवियों का एक संकलन था – जिसमें नई कविता का बीज बोया गया। अज्ञेय ने भूमिका में लिखा:
“कविता को प्रयोग की भूमि मानना चाहिए।”
यह कथन हिंदी कविता के नए युग का घोषणापत्र बन गया।
3. काव्य भाषा और प्रतीक प्रयोग
अज्ञेय की कविता की भाषा संयत, विचारशील और प्रतीकात्मक होती है। उदाहरण:
“विपथगा!
सघन पंथ-वल्गा को
छोड़ तू अनबँधे पथ की
परिकल्पना बन।”
यहाँ मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, बंधनों से मुक्ति और नई राहों की तलाश को व्यक्त किया गया है।
4. विषयों की विविधता
अज्ञेय की कविताएँ दर्शन, अस्तित्ववाद, मनोविज्ञान, युद्ध, विज्ञान और सांस्कृतिक चिंतन जैसे विषयों को उठाती हैं – जो हिंदी कविता के लिए एक नई जमीन थी।
5. आत्मसंघर्ष और निजी अनुभव
उनकी कविता में बाह्य समाज के बजाय आंतरिक यथार्थ की खोज अधिक है। जैसे:
“यह मैं हूँ –
जल में अपनी ही परछाईं
ताकता – डूबता – उठता।”
यह प्रतीक आधुनिक मनुष्य की आत्मचेतना और पहचान की उलझन को दर्शाता है।
निष्कर्ष
प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया, और इस आंदोलन के सर्वप्रमुख सूत्रधार अज्ञेय थे। उन्होंने कविता को बौद्धिकता, अनुभव की विविधता, प्रतीकात्मकता और विचारशीलता से समृद्ध किया। उनकी भूमिका केवल एक कवि की नहीं, बल्कि एक दृष्टा, संपादक और पथप्रदर्शक की थी, जिन्होंने आने वाले नव-काव्य आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।