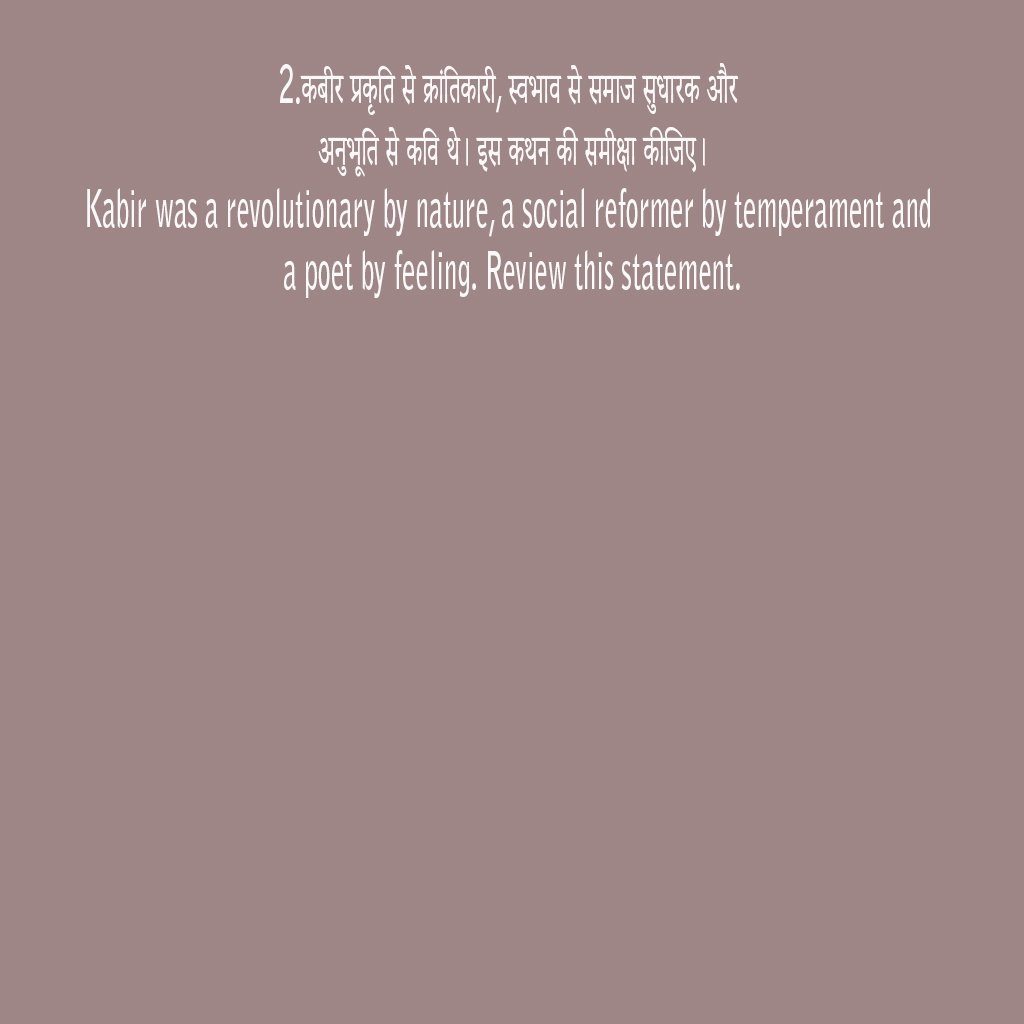कबीर प्रकृति से क्रांतिकारी स्वभाव से समाज सुधारक और अनुभूति से कवि Kabir was a revolutionary by nature a social reformer by temperament and a poet by spirit.
शुरू से अंत तक पढ़ें।
1. भूमिका
भारतीय संत परंपरा में कबीर का नाम अत्यंत सम्मान और प्रेरणा से लिया जाता है। वे ऐसे कवि थे, जिन्होंने धार्मिक पाखंड, जातिवाद और सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध एक जोरदार आवाज उठाई। कबीर न केवल एक भक्त संत थे, बल्कि वे सामाजिक सुधारक, क्रांतिकारी विचारक और एक अनुभूतिपरक कवि भी थे।
“कबीर प्रकृति से क्रांतिकारी, स्वभाव से समाज सुधारक और अनुभूति से कवि थे” – यह कथन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को तीन स्तरों पर अभिव्यक्त करता है:
- क्रांतिकारी के रूप में वे परंपरागत धार्मिक आडंबरों के खिलाफ खड़े हुए।
- समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जातिवाद, ऊँच-नीच, मूर्तिपूजा और ढकोसले का विरोध किया।
- कवि के रूप में उन्होंने अपने अनुभवों, चेतना और भक्ति को साखी, रमैनी और सबद के माध्यम से व्यक्त किया।
इस उत्तर में हम इस कथन के प्रत्येक अंश की समीक्षा विस्तृत रूप में करेंगे।
2. कबीर: प्रकृति से क्रांतिकारी
2.1 धार्मिक क्रांति के प्रणेता
कबीर का युग 15वीं शताब्दी का था, जब भारत में भक्ति आंदोलन चरम पर था और साथ ही समाज धार्मिक आडंबरों, पाखंड, जातिगत भेदभाव और बाह्याचारों से ग्रस्त था। कबीर ने दोनों प्रमुख धर्मों – हिंदू और इस्लाम – की आलोचना की और केवल एक निराकार परमात्मा की उपासना को ही श्रेष्ठ बताया।
उनके कुछ प्रसिद्ध पदों से उनकी क्रांतिकारी प्रकृति स्पष्ट होती है:
माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर॥
यहाँ कबीर ने बाह्य पूजा और प्रतीकों की असारता पर सवाल खड़ा किया। उनकी कविताएँ एक जागरण का शंखनाद थीं।
2.2 दोनों धर्मों की आलोचना
कबीर ने हिंदू और मुसलमान – दोनों के धार्मिक कृत्यों पर चोट की।
पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार।
ताते तो चाकी भली, पीस खाय संसार॥
कांकर पाथर जोड़ि के मस्जिद लई बनाय।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय?
ये पंक्तियाँ उस समय के धार्मिक ढाँचे पर सीधी चोट थीं। कबीर ने दिखाया कि सच्चा धर्म हृदय की पवित्रता में होता है, न कि मूर्तियों या मस्जिदों में।
2.3 निराकार ब्रह्म का प्रचारक
कबीर ने ब्रह्म को निराकार माना और भक्ति को व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित बताया। वे ‘राम’ नाम के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करते थे, पर उनका राम दशरथ का पुत्र नहीं, बल्कि एक अव्यक्त, निर्गुण सत्ता था।
राम रहीम एक हैं, नाम धराया दोय।
कहै कबीर सुनो भइ साधो, गुरु गोविंद न होय॥
यह चिंतन कबीर को साधारण संत से अलग करता है और उन्हें धार्मिक क्रांतिकारी बनाता है।
3. कबीर: स्वभाव से समाज सुधारक
कबीर न केवल धार्मिक विचारों के विरोधी थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी गहरा प्रहार किया। उनका जीवन और साहित्य सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध एक क्रांति थी।
3.1 जाति प्रथा का विरोध
कबीर ने जाति व्यवस्था को मानव समाज का सबसे बड़ा अभिशाप माना और उसका प्रबल विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं।
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान॥
वे कहते हैं कि समाज व्यक्ति की जाति नहीं, बल्कि उसके गुण, ज्ञान और कर्म को महत्व दे।
3.2 ब्राह्मणवाद पर आक्रमण
कबीर ने विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग की उस मानसिकता का विरोध किया जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का दावा करती थी:
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार,
ताते तो चाकी भली पीस खाय संसार।
कबिरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर।
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर॥
उनका यह विचार आज के समतावादी लोकतंत्र की भी नींव में पाया जाता है।
3.3 स्त्रियों और श्रमिक वर्ग की चेतना
कबीर ने स्त्रियों की गरिमा और श्रमिक वर्ग की पीड़ा को समझा। उन्होंने सूत कातने, जुलाहे का कार्य करने जैसी गतिविधियों को आध्यात्मिकता से जोड़ा।
दास कबीर जतन करि ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
यह प्रतीक है श्रम की शुद्धता और संतोष की भावना का।
4. कबीर: अनुभूति से कवि
कबीर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अनुभव की भूमि पर खड़ा है। वे किसी शास्त्रीय विद्वता के नहीं, आत्मिक अनुभूति के कवि हैं। उन्होंने जैसा देखा, जैसा जिया, वैसा ही लिखा।
4.1 कबीर की भक्ति: निर्गुण और अनुभव आधारित
कबीर की भक्ति निर्गुण थी – जिसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं। वह व्यापक, निराकार और सर्वत्र व्याप्त था।
जहाँ देखूं तहाँ तू ही तू, और न दूजा कोई।
तेरे अंदर तू है, मेरे अंदर तू॥
यह भावना उन्हें किसी भी तरह की बाह्य साधना से दूर ले जाती है। उनका ईश्वर हृदय में है, मंदिर-मस्जिद में नहीं।
4.2 शैली और भाषा
कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी – जिसमें ब्रज, अवधी, खड़ीबोली, अरबी-फारसी और लोकबोलियों का मिश्रण था। उनका काव्य लोकबोध से भरा हुआ है, और सीधी-सादी भाषा में गहरी बात कहने की अद्भुत क्षमता रखता है।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय॥
यह आत्मनिरीक्षण और दर्शन दोनों का अनूठा संगम है।
4.3 रूपात्मकता और प्रतीक
कबीर ने अपने काव्य में अनेक रूपक, प्रतीक और दृष्टांतों का प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में चादर, धागा, जुलाहा, सूत, पानी, नाव आदि प्रतीकों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक विचारों को सरलता से व्यक्त किया गया।
जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग।
तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग॥
यह अनुभव आधारित कविता है, जिसमें कबीर आत्मसाक्षात्कार की प्रेरणा दे रहे हैं।
5. कबीर की प्रासंगिकता
कबीर केवल अपने युग के नहीं, बल्कि हर युग के कवि और विचारक हैं। आज भी जब समाज जातिवाद, धर्म के नाम पर हिंसा, पाखंड और भेदभाव से जूझ रहा है, तब कबीर की वाणी प्रकाश पुंज की तरह है।
- उन्होंने धर्म की आत्मा को जगाया, न कि उसकी बाहरी परतों को।
- उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश दिया।
- उनका साहित्य लोकचेतना और मानवता का साहित्य है।
6. कबीर के आलोचकों की दृष्टि
कुछ आलोचकों ने कबीर की रचनाओं में ‘कटुता’ और ‘आक्रोश’ के तत्व देखे हैं। वे मानते हैं कि कबीर की वाणी कभी-कभी उग्र और अपमानजनक हो जाती है। परंतु यह भी सत्य है कि उनका यह तीव्र तेवर उस समय की धर्म-संस्कृति में व्याप्त अन्याय और रूढ़ियों के विरुद्ध था।
डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर को “जाग्रत आत्मा” कहा है – जो समाज को झकझोरने के लिए बाध्य थी। उनका कहना था –
**“कबीर की भाषा तलवार की तरह है – वह वार करती है, पर घायल करने के लिए नहीं, झकझोर कर
जगा देने के लिए।”**
7. निष्कर्ष
“कबीर प्रकृति से क्रांतिकारी, स्वभाव से समाज सुधारक और अनुभूति से कवि थे” – यह कथन कबीर के त्रैतीय आयामों को समेटता है:
- प्रकृति से क्रांतिकारी – क्योंकि उन्होंने धार्मिक कट्टरता और बाह्याचारों के खिलाफ बगावत की।
- स्वभाव से समाज सुधारक – क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊँच-नीच, छुआछूत, पाखंड और आडंबर का विरोध किया।
- अनुभूति से कवि – क्योंकि उनके शब्द किताबों से नहीं, जीवन की सच्चाई और आत्मा की गहराइयों से निकलते हैं।
उनकी वाणी आज भी उतनी ही ताजगी और सच्चाई के साथ हमारे हृदय को स्पर्श करती है, जितनी उनके समय में।