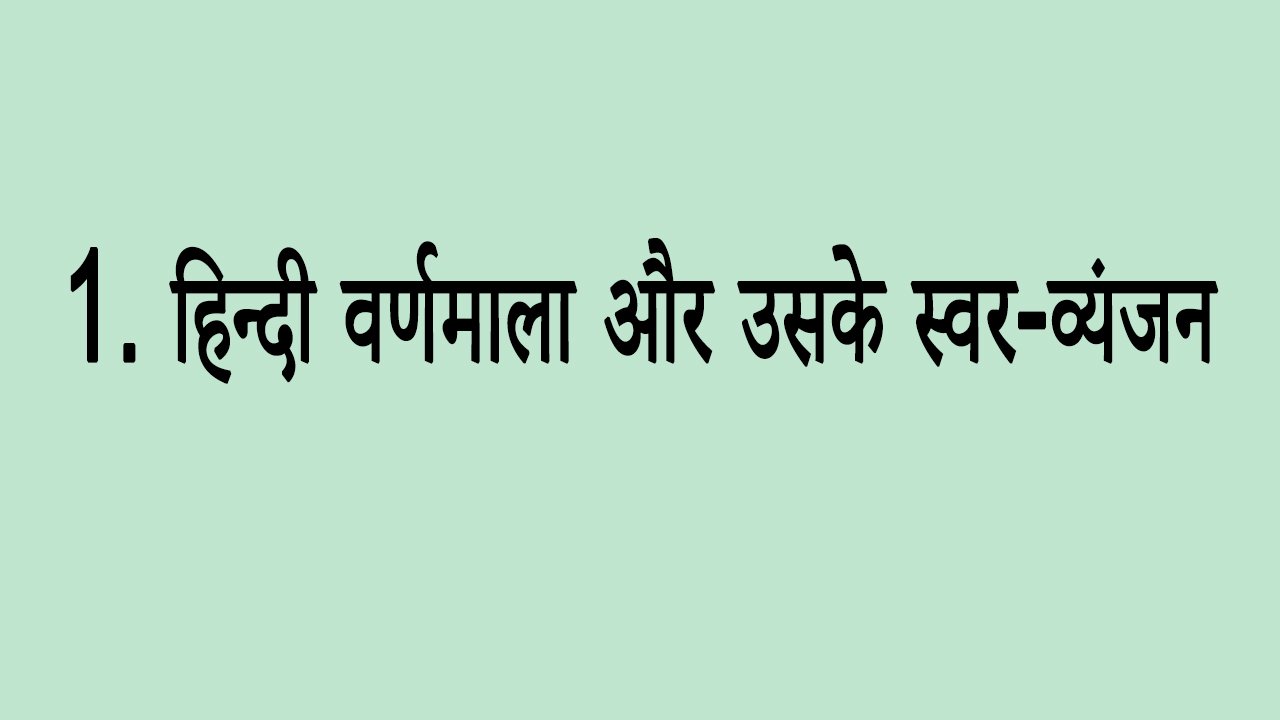1. हिन्दी वर्णमाला और उसके स्वर-व्यंजन
हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अन्य वर्ण (अयोगवाह और अनुस्वार) शामिल होते हैं।
स्वर-
स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।
– मूल स्वर- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ
– संयुक्त स्वर- अं (अनुस्वार), अः (विसर्ग)
व्यंजन- 1. हिन्दी वर्णमाला और उसके स्वर-व्यंजन
व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं है। इन्हें मुख के विभिन्न भागों के उपयोग के आधार पर 5 वर्गों में बाँटा गया है-
– क-वर्ग- क, ख, ग, घ, ङ
– च-वर्ग- च, छ, ज, झ, ञ
– ट-वर्ग- ट, ठ, ड, ढ, ण
– त-वर्ग- त, थ, द, ध, न
– प-वर्ग- प, फ, ब, भ, म
– अव्यवहित व्यंजन- य, र, ल, व, श, ष, स, ह
—
2. संधि और संधि-विच्छेद
संधि का अर्थ है दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण या शब्द बनना।
संधि के प्रकार-
1. स्वर संधि- स्वर से स्वर का मेल (जैसे, राम + ईश = रामेश)
2. व्यंजन संधि- व्यंजन और स्वर/व्यंजन का मेल (जैसे, विद्या + आलय = विद्यालय)
3. विसर्ग संधि- विसर्ग (ः) से स्वर/व्यंजन का मेल (जैसे, दुःख + हार = दु-खार्द्र)
संधि-विच्छेद-
संधि-विच्छेद में संधि किए गए शब्द को तोड़कर मूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे, ‘पुनः + आगमन = पुनरागमन’।
—
3. समास और उसके प्रकार
समास का अर्थ है दो या अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप में एक साथ आना।
समास के प्रमुख प्रकार-
1. तत्पुरुष समास- एक शब्द प्रधान होता है। (जैसे, राजपुत्र = राजा का पुत्र)
2. कर्मधारय समास- दोनों शब्द समान होते हैं। (जैसे, नीलगगन = नीला गगन)
3. द्वंद्व समास- दोनों शब्द समान महत्व के होते हैं। (जैसे, राम-लक्ष्मण)
4. बहुव्रीहि समास- जिसका अर्थ दोनों शब्दों से अलग हो। (जैसे, पीतांबर = पीला वस्त्र पहनने वाला)
5. अव्ययीभाव समास- पहला शब्द अव्यय होता है। (जैसे, तुरंतप्रकाश = तुरंत प्रकाश)
—
4. क्रिया, विशेषण और सर्वनाम
क्रिया-
क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है।
– भूतकाल- मैंने खाया।
– वर्तमानकाल- मैं खा रहा हूँ।
– भविष्यकाल- मैं खाऊँगा।
विशेषण-
विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है।
– जैसे, सुंदर फूल (सुंदर = विशेषण)
सर्वनाम-
सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
– जैसे, वह, यह, मैं, तुम, हमारा।
—
5. वाक्य रचना और वाक्य प्रकार
वाक्य रचना-
हिन्दी वाक्य में सामान्य क्रम होता है- कर्ता + कर्म + क्रिया।
उदाहरण- राम ने गेंद खेली।
वाक्य प्रकार-
1. नियमवाचक वाक्य- जिसमें सामान्य जानकारी दी जाए। (जैसे, बच्चा पढ़ रहा है।)
2. प्रश्नवाचक वाक्य- जिसमें प्रश्न पूछा जाए। (जैसे, क्या आप आएंगे?)
3. आज्ञावाचक वाक्य- जिसमें आदेश, निवेदन, या सलाह दी जाए। (जैसे, कृपया बैठ जाइए।)
4. विस्मयादिबोधक वाक्य- जिसमें आश्चर्य, खुशी या दुःख प्रकट हो। (जैसे, अरे! क्या सुंदर दृश्य है।)
—
6. कारक और विभक्ति
कारक-
कारक संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में संबंध को दर्शाते हैं। हिन्दी में 8 कारक होते हैं-
1. कर्ता- कर्म करने वाला।
2. कर्म- जिस पर कार्य हो।
3. करण- जिसके द्वारा कार्य हो।
4. संप्रदान- जिसे कार्य सौंपा जाए।
5. अपादान- जिससे अलगाव हो।
6. सम्प्रयोग- जो साथ हो।
7. अधिकरण- जिसमें कार्य हो।
8. संबोधन- पुकारने के लिए।
विभक्ति-
विभक्ति का प्रयोग कारक के साथ होता है और वह वाक्य में शब्दों को जोड़ने का काम करता है।
उदाहरण-
– राम ने खाना खाया। (कर्ता कारक – विभक्ति ‘ने’)
– मैंने पुस्तक को पढ़ा। (कर्म कारक – विभक्ति ‘को’)
—
इन टॉपिक्स पर अगर और भी गहराई से जानकारी चाहिए, तो बताइए!
READ ALSO – बालगोबिन भगत पाठ में भगतजी के व्यक्तित्व के कौन-कौन से गुण उभरकर आते हैं